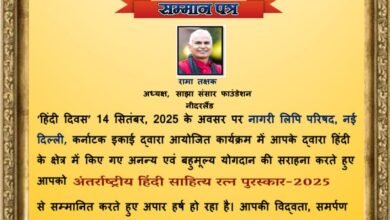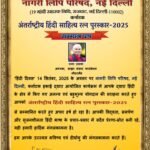आलेख – स्वतन्त्रता
लेखक- योगेश गहतोड़ी जी
- प्रस्तावना-
मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल उसके भौतिक अस्तित्व में नहीं निहित है, अपितु उसकी आत्मा की पूर्णता, तृप्ति और मोक्ष में ही उसकी वास्तविक उपलब्धि है। यह आत्मिक उपलब्धि केवल सांसारिक साधनों या अधिकारों से नहीं, बल्कि उस गहन चेतना से प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में मनुष्य जिन चार मूलभूत प्रेरणाओं “सुरक्षा, सम्मान, सुख और स्वतन्त्रता” से संचालित होता है। इन्हें वैदिक दृष्टिकोण में कामना चतुष्टय कहा गया है। ये चारों कामनाएँ जीवन के क्रमिक विकास की सीढ़ियाँ हैं, जो व्यक्ति को स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल भोग से आत्मिक बोध की ओर ले जाती हैं।
इनमें अन्तिम और सर्वोच्च अवस्था ‘स्वतन्त्रता है। यह केवल किसी राजनीतिक या सामाजिक दशा का संकेत नहीं देती, अपितु यह आत्मा की वह शुद्धतम, स्वशासित और ब्रह्मस्वरूप स्थिति है, जहाँ कोई इच्छा शेष नहीं रहती, कोई बंधन शेष नहीं होता और आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। यही कारण है कि स्वतंत्रता को आत्मिक उन्नति की परम परिणति कहा गया है।
- स्वतन्त्रता की विवेचना-
‘स्वतन्त्रता ’ शब्द संस्कृत के ‘स्व’ (अर्थात् आत्मा, निजता, निजस्वरूप) और ‘तन्त्र’ (अर्थात् शासन, व्यवस्था या नियंत्रण) शब्दों से मिलकर बना है। इसका मूल तात्पर्य है— वह तंत्र जो किसी बाहरी सत्ता पर आश्रित न होकर स्वयं से उत्पन्न हो, जो आत्मा के विवेक और ज्ञान से संचालित हो। इस दृष्टिकोण से स्वतन्त्रता का सम्बन्ध केवल बाह्य मुक्ति से नहीं है, बल्कि उस आन्तरिक स्थिति से है, जहाँ आत्मा स्वयं को संचालित करती है, आत्मनिर्भर होती है और किसी अन्य की सत्ता की आवश्यकता अनुभव नहीं करती है।
वेद, उपनिषद और भगवद्गीता इस स्वतन्त्रता को विविध नामों से संबोधित करते हैं—मोक्ष, कैवल्य, अमृतत्व, निर्वाण आदि। कठोपनिषद में एक अत्यंत सूक्ष्म सूत्रवाक्य में कहा गया है— “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः” अर्थात् अमृतत्व या पूर्ण स्वतन्त्रता केवल त्याग और आत्मज्ञान से प्राप्त की जाती है। यह धन, वंश या कर्मफल से नहीं मिल सकता है। इस उद्घोष के माध्यम से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता कोई बाहरी उपार्जन नहीं, बल्कि आत्मा की उस स्थिति की पुनःप्राप्ति है, जिसमें वह सदा से थी, परंतु जिसे वह विस्मरण के कारण खो बैठी है।
- स्वतन्त्रता के प्रकार
स्वतंत्रता को दो मुख्य स्तरों पर समझा जा सकता है— एक बाह्य स्वतन्त्रता और दूसरी आन्तरिक स्वतन्त्रता।
बाह्य स्वतन्त्रता वह दशा है, जहाँ व्यक्ति किसी शासन, परंपरा, समाज, परिवार या संस्था के जबरदस्त नियंत्रण से मुक्त होकर अपने विचारों, कर्मों और जीवनपथ का स्वतन्त्र चुनाव कर सकता है। इसमें भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित होते हैं। यह आधुनिक मानवाधिकारों और लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं का मूल आधार है। यद्यपि यह स्वतंत्रता अनिवार्य है, परन्तु यदि इसे विवेक और कर्तव्यबोध से नहीं जोड़ा गया तो यह स्वतन्त्रता स्वेच्छाचार में परिवर्तित होकर सामाजिक विघटन का कारण बन सकती है।
आन्तरिक स्वतन्त्रता वह सूक्ष्म और आत्मिक अवस्था है, जिसमें आत्मा सभी मानसिक और आध्यात्मिक बन्धनों से मुक्त हो जाती है। जैसे राग-द्वेष, भय, मोह, वासना, अहंकार और अज्ञान। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष “अयं आत्मा ब्रह्म” (यह आत्मा ही ब्रह्म है) आन्तरिक स्वतन्त्रता की घोषणा करता है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति में “अहं ब्रह्मास्मि” का जागरण होता है और वह जान लेता है कि वह न कर्ता है, न भोक्ता, न पीड़ित, न परतन्त्र है, वह केवल ब्रह्म है। इस स्थिति में पहुँचकर व्यक्ति न मोक्ष की कामना करता है, न ही जीवन से पलायन करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि स्वतन्त्रता उसका मूलस्वरूप है।
- स्वतन्त्रता: भारत की आत्मा और विश्व का आलोक-
भारत के लिए स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की जागृत चेतना रही है। वैदिक ऋचाओं, उपनिषदों, संतों की समदृष्टि और गांधी के सत्याग्रह में सतत प्रवाहित होती हुई। 15 अगस्त 1947 को प्राप्त स्वतंत्रता सत्ता परिवर्तन से अधिक एक आत्मिक पुनर्जन्म थी, जहाँ ऋषियों का स्वराज्य-बोध, बुद्ध-महावीर की मुक्ति साधना और स्वतन्त्रता सेनानियों का त्याग यह सब एक सांस्कृतिक जागरण का स्वर बन गए। गांधी ने स्वतन्त्रता को सत्य, अहिंसा और आत्मबल की साधना कहा, जिसे संविधान ने अधिकार और कर्तव्य के संतुलन में रूप दिया। आज, जब भारत विज्ञान और वैश्विक संवाद के युग में है, स्वतंत्रता केवल बाह्य स्वायत्तता नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, सेवा और साधना से युक्त एक आलोकमय कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि अरविंद जी ने कहा था कि भारत एक दिन आध्यात्मिक विश्वगुरु के रूप में स्वतंत्रता के दीप से समस्त मानवता को आलोकित करेगा। - स्वतन्त्रता: बाल्यकाल से आत्मजागरण तक-
स्वतन्त्रता की भावना मानव जीवन में अचानक नहीं आती, यह एक क्रमिक विकास है जो बचपन से शुरू होकर परिपक्वता और अंततः आत्मजागरण तक पहुँचती है। बचपन में इसका रूप भयमुक्त खेल और जिज्ञासा होता है। किशोरावस्था में स्वीकृति की चाह; युवावस्था में प्रयोग और स्वनिर्णय की आकांक्षा, लेकिन यदि यह भावना आत्मनियंत्रण और विवेक से शून्य हो, तो यह भ्रम का रूप ले लेती है। परिपक्वता में वही स्वतन्त्रता सार्थक बनती है, जब व्यक्ति ‘जो सही है, वही करने’ की क्षमता प्राप्त करता है। यही आत्मनुशासित स्वतंत्रता सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। - प्रकृति में निहित स्वतन्त्रता-
स्वतन्त्रता केवल आत्मा की मुक्ति या राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ संतुलन और समरसता की भी मांग करती है। जब मनुष्य अपने कर्मों से प्रकृति के सनातन नियमों — जिन्हें वैदिक परम्परा में ‘ऋत’ कहा गया है — का उल्लंघन करता है, तो वह न केवल पर्यावरण को बाधित करता है, बल्कि अपनी आंतरिक स्वतंत्रता भी खो देता है। ऋत, केवल भौतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नैतिकता और सांस्कृतिक अनुशासन का प्रतीक है। वैदिक ऋषियों के अनुसार वही मनुष्य स्वतंत्र है, जो प्रकृति के साथ तादात्म्य रखता है और सह-अस्तित्व की भावना से जीवन जीता है। जो हमें ‘ऋत’ की मर्यादा में रहकर आत्म-अनुशासन और सृष्टि के साथ सामंजस्य की ओर ले जाए, वही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। - स्वतन्त्रता और शान्ति का संबंध-
स्वतंत्रता और शान्ति का सम्बन्ध गहराई से आत्मिक और नैतिक है। जब व्यक्ति या समाज सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है, तब वह भय, लोभ, मोह और अधर्म के बंधनों से मुक्त होता है। केवल तभी वह आंतरिक और बाह्य शान्ति का वास्तविक अनुभव कर सकता है। वैदिक दृष्टिकोण में स्वतन्त्रता मात्र किसी अधिकार या स्वायत्तता का नाम नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहाँ आत्मा अपनी स्वधीनता में स्थित होती है, और यही स्वधीनता शांति की भूमि बनती है।
जहाँ मन की चंचलता शांत होती है, कर्म ऋत (सृष्टि-संगत नैतिकता) के अनुसार होता है और जीवन उत्तरदायित्व से प्रेरित होता है — वहीं स्थायी शांति निवास करती है। इसीलिए वैदिक परंपरा में स्वतंत्रता की कामना के साथ प्रायः शांति मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे:
ॐ द्यौः शान्तिः — स्वर्ग (ऊपरी आकाश) में शांति हो।
अन्तरिक्षं शान्तिः — मध्य आकाश (वायुमंडल) में शांति हो।
पृथिवी शान्तिः — धरती पर शांति हो।
आपः शान्तिः — जल में शांति हो।
औषधयः शान्तिः — औषधियों (वन की जड़ी-बूटियों) में शांति हो।
वनस्पतयः शान्तिः — पेड़ों, पौधों और वनस्पतियों में शांति हो।
विश्वे देवा: शान्तिः — सभी देवताओं (प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों) में शांति हो।
ब्रह्म शान्तिः — ब्रह्म (परब्रह्म/सत्य) में शांति हो।
सर्वं शान्तिः — समस्त जगत और समस्त अस्तित्व में शांति हो।
शान्तिरेव शान्ति श — शान्ति ही शांति हो; केवल शांति का ही विस्तार हो।
सा मा शान्तिरेधि — वह शान्ति मेरे भीतर भी आकर स्थापित हो।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः — त्रिविध तापों (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक) से मुक्ति की प्रार्थना।
भावार्थ:- यह मन्त्र समस्त सृष्टि में सार्वभौमिक शांति की कामना करता है — जहाँ कोई अशांति, द्वंद्व, हिंसा या विक्षोभ न हो। व्यक्ति और प्रकृति के बीच सन्तुलन, सौम्यता और सह-अस्तित्व का भाव ही वैदिक शान्ति का आदर्श है।
अतः बिना आन्तरिक सन्तुलन और आत्म-नियंत्रण के कोई भी स्वतंत्रता केवल उथल-पुथल और असंतुलन को जन्म देती है। जब स्वतन्त्रता विवेक, मर्यादा और सह-अस्तित्व से जुड़ी होती है, तभी वह व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वभौमिक स्तर पर शान्ति को जन्म देती है और यही सच्ची स्वतंत्रता की पूर्णता है।
- भगवद्गीता में स्वतन्त्रता की अवधारणा*
भगवद्गीता में स्वतन्त्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और आत्मनिर्भरता का प्रतिफल है। श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं—
“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥”
अर्थ:- मनुष्य को स्वयं ही अपने आत्मा द्वारा उद्धार करना चाहिए; आत्मा ही उसकी मित्र है और वही शत्रु भी बन सकती है। यह कथन स्वतंत्रता को केवल बाह्य स्वतन्त्रता के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन आत्मिक उत्तरदायित्व के रूप में प्रस्तुत करता है।
गीता में एक और स्थान पर श्रीकृष्ण कहते हैं—
“विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥”
अर्थात् जो समस्त इच्छाओं को त्यागकर निःस्पृह, निर्मम और निरहंकारी हो जाता है, वही परम शान्ति को प्राप्त करता है। यह शांति ही सच्ची स्वतंत्रता है, जो आत्मबोध, आत्म-नियन्त्रण और आत्म-निष्ठा से प्राप्त होती है। गीता के अनुसार, स्वतंत्रता कोई अधिकार नहीं, जिसे कोई सरकार दे सकती है। यह वह शक्ति है जो केवल योग, तप और आत्मबोध के माध्यम से आत्मा के भीतर से प्रकट होती है।
- आधुनिक चिन्तन में स्वतन्त्रता का बोध-
आधुनिक विचारकों ने स्वतन्त्रता को केवल राजनीतिक स्वायत्तता नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण के रूप में देखा है। स्वामी विवेकानन्द जी के अनुसार, “प्रत्येक आत्मा मूलतः दिव्य है” और जीवन का लक्ष्य उसी अन्तर्निहित दिव्यता को प्रकट करना है। उनके अनुसार, “मुक्ति ही सम्पूर्ण प्रकृति का अन्तिम लक्ष्य है।” वहीं महर्षि अरविंद जी का मानना था कि आत्मा की आन्तरिक स्वतन्त्रता ही सच्चे स्वराज्य की नींव है। वह भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र मानते थे, जिसका उद्देश्य है — “विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश देना।” इन दोनों महापुरुषों के अनुसार, सच्ची स्वतन्त्रता वही है, जो आत्मा को भीतर से प्रकाशित करती है और जब आत्मा आलोकित होती है, तभी समाज और राष्ट्र भी प्रकाशमय बनते हैं।
10. स्वतन्त्रता और उत्तरदायित्व
सच्ची स्वतन्त्रता वही होती है, जो कर्तव्य और धर्मबोध से जुड़ी हो। अगर स्वतन्त्रता में केवल अधिकारों की बात हो और उत्तरदायित्व का बोध न हो, तो वह स्वेच्छाचार का रूप ले लेती है और समाज के पतन का कारण बनती है। एक ऋषि का त्याग, राजा का न्याय और गृहस्थ का अनुशासन; यह सब स्वतन्त्रता के ही विभिन्न रूप हैं, जो धर्म, विवेक और कर्तव्य पर आधारित होते हैं। जब स्वतन्त्रता आत्मविवेक, आत्मानुशासन और समाज के हित से जुड़ती है, तब वह न केवल व्यक्ति को आत्मिक ऊँचाइयों तक ले जाती है, बल्कि समाज को भी स्थिरता और दिशा प्रदान करती है। ऐसी स्वतन्त्रता व्यक्ति को ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर करती है और समाज को सुदृढ़ बनाती है।
- स्वतन्त्रता और भक्ति-
स्वतन्त्रता का सम्बन्ध केवल बाह्य परिस्थितियों से नहीं, बल्कि प्राणमय अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ा होता है। योगदर्शन में इसे ‘कैवल्य’ कहा गया है। जहाँ आत्मा सम्पूर्ण प्रकृति से विलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। भक्ति परंपरा में यही स्थिति आत्मलीनता के रूप में प्रकट होती है, जब भक्त ईश्वर में पूर्ण समर्पण के साथ लीन होकर समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है। यह स्वतन्त्रता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि समष्टि चेतना से भी जुड़ी होती है, जब व्यक्ति लोकमंगल के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। इस प्रक्रिया में ज्ञान वह दीपक है, जो विवेक का आलोक देता है और आत्मा को विकल्पहीन शांति की अवस्था तक ले जाता है। इसीलिए कहा गया है — “स्वतन्त्रता केवल विकल्पों की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मा की विकल्पहीन स्थिति है।” जब यह दीपक भीतर जलता है, तो “यह दीप केवल हमें प्रकाशित नहीं करता, अपितु हमसे संपूर्ण जगत को प्रकाशित कराता है”, यही असली स्वतन्त्रता है। - अद्वैत वेदांत में स्वतंत्रता-
अद्वैत वेदांत के अनुसार बंधन का मूल कारण अविद्या अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है। जब जीव स्वयं को कर्ता, भोक्ता और जगत का आश्रित मानता है, तभी वह कर्मबंधन में उलझता है; परंतु जब उसे ब्रह्मज्ञान होता है, तब वह समझता है कि वह न कर्ता है, न भोक्ता और न ही कोई पृथक सत्ता है। शंकराचार्य द्वारा उद्घोषित “तत्त्वमसि”, “अहं ब्रह्मास्मि” और “नेति नेति”* जैसे महावाक्य व्यक्ति को उसकी आत्मस्वरूपता की स्मृति कराते हैं।
जब यह ज्ञान आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह स्वतः जान जाती है कि वह सदा से मुक्त थी, है और रहेगी। उसे न किसी मोक्ष की कामना रहती है, न किसी बन्धन की चिन्ता रहती है। यही स्वरूपसिद्धि है, जो स्वतन्त्रता की चरम अवस्था है। इस स्थिति में आत्मा निर्विकल्प, निर्विकार और नित्य शांति में स्थित हो जाती है, जिसे ब्रह्मस्थिति कहा गया है।
- कामना चतुष्टय में स्वतन्त्रता का स्थान-
कामना चतुष्टय जीवन के विकास की एक प्राकृतिक और क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें—
(क) सुरक्षा- शरीर की रक्षा और स्थायित्व की कामना है।
(ख) सम्मान- मन की स्वीकृति और सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा है।
(ग) सुख- चित्त की तृप्ति और भावनात्मक समरसता की आकांक्षा है।
(घ) स्वतन्त्रता- आत्मा की पूर्णता और मुक्ति की अभिव्यक्ति है।
इनमें स्वतन्त्रता ही वह अवस्था है, जहाँ आत्मा किसी बाह्य सत्ता से नहीं, अपितु अन्तर्विकारों से भी पूर्णतः मुक्त हो जाती है। यह अवस्था आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जिसमें वह स्वयं में स्थित होकर ब्रह्म का अनुभव करती है। यही आत्म-बोध की चरम स्थिति है और यही जीवन का परम लक्ष्य भी है।
- स्वतन्त्रता- कामना चतुष्टय का अन्तिम दीप-
कामना चतुष्टय का अन्तिम दीप “स्वतन्त्रता” केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मा की परम उपलब्धि और उसकी स्वाभाविक स्थिति है। यह वह दिव्य ज्योति है जहाँ समस्त सांसारिक कामनाएँ सुरक्षा, सम्मान, सुख अंततः शांत हो जाती हैं और आत्मा अपने स्वरूप, अपने स्व, में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह कोई बाह्य उपलब्धि या सामाजिक स्थिति नहीं है, बल्कि आत्मा की वह मौलिक, शुद्ध और निर्विकार स्थिति है, जहाँ न कोई भय रहता है, न कोई इच्छा, न द्वन्द्व और न ही किसी प्रकार का बन्धन। यह स्थिति केवल एक अंत नहीं, बल्कि पूर्णता की वह अवस्था है, जहाँ अस्तित्व स्वयं में पूर्ण, स्वतन्त्र, आत्म-प्रकाशित और सन्तुष्ट होता है।
भगवद्गीता के एक श्लोक के अनुसार —
“सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
*अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥”
— भगवद्गीता, अध्याय 18, श्लोक 66
अर्थ:- इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी कर्तव्यों और बंधनों को त्यागकर मेरी शरण में आओ। ‘सर्वधर्म’ का त्याग यहाँ कर्तृत्व के अहंकार और फल की आसक्ति को छोड़ने का संकेत है। जब मनुष्य पूर्ण समर्पण से ईश्वर को अपनाता है, तभी वह पापों और बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष अर्थात् आत्मा की पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त करता है। सच्ची स्वतन्त्रता, ईश्वर की शरण और द्वंद्वों से मुक्त चित्त में ही संभव है।
- उपसंहार-
स्वतन्त्रता कोई क्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा की वह सनातन पुकार है, जो जीवन के प्रत्येक चरण — सुरक्षा, सम्मान, सुख और अंततः ब्रह्मबोध में निरन्तर गूँजती रहती है। यह केवल अधिकारों की चकाचौंध नहीं, अपितु कर्तव्यों की आन्तरिक तपश्चर्या है, जो आत्मानुशासन से जन्म लेती है, आत्मबोध से प्रकाशित होती है और ऋत-संगत जीवन में अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। कामना चतुष्टय के अंतिम दीप के रूप में स्वतन्त्रता वह शिखर अवस्था है, जहाँ आत्मा भय, मोह, वासना और अहंकार के अन्धकार से मुक्त होकर ब्रह्मस्वरूप आलोक में स्थित हो जाती है। यह वही अनुभूति है, जहाँ “अहं ब्रह्मास्मि” की चेतना व्यक्ति को बंधनों से नहीं, बल्कि समष्टि और सृष्टि से एकात्म करती है। भारत की स्वतन्त्रता भी इसी आत्मिक पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति रही है, जहाँ वेदों की ऋचाएँ, ऋषियों का त्याग, संतों की समदृष्टि, स्वतन्त्रता सेनानियों की आहुति और संविधान की मर्यादाएँ यह सभी मिलकर एक ऐसा दीप जलाते हैं, जो केवल भारत ही नहीं, अपितु समस्त मानवता को आलोकित करता है।
अतः सच्ची स्वतन्त्रता के लिए एक वैदिक प्रार्थना के माध्यम से कहा गया है —
“ॐ स्वातंत्र्यं ब्रह्मरूपं मे अस्तु। शान्तिर्मे अस्तु। आत्मा मे स्वधीनो भवतु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥”
अर्थात् — “मेरी स्वतन्त्रता ब्रह्मस्वरूप हो,” मेरी मुक्ति केवल बाह्य बन्धनों से नहीं, बल्कि आत्मा की उस शुद्ध, निरपेक्ष और ब्रह्म-तुल्य अवस्था से हो जहाँ कोई द्वन्द्व न रहे। “मेरे भीतर शान्ति हो,” अर्थात् सभी आन्तरिक विकार, क्लेश और अशान्ति समाप्त होकर आत्मा विश्रान्ति प्राप्त करे। “मेरी आत्मा स्वधीन हो,” अर्थात् वह किसी लोभ, भय, मोह या बाह्य सत्ता से नियन्त्रित न होकर आत्मज्ञान के आलोक में स्वयं का संचालन स्वयं करे। अन्त में — “ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः” — त्रिविध तापों (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक) से मुक्ति और सम्पूर्ण अस्तित्व में गहन, स्थायी शांति की मंगलकामना है। यह प्रार्थना आत्ममुक्ति, आत्मनियंत्रण और ब्रह्मत्व की उस दिव्य अवस्था की अभिलाषा है, जहाँ स्वतन्त्रता केवल सामाजिक स्थिति नहीं, आत्मा की पूर्ण और जागृत अनुभूति बन जाती है।
साभार संकलित-
पं० जुगल किशोर त्रिपाठी (साहित्यकार)
बम्हौरी, मऊरानीपुर, झाँसी (उ०प्र०)