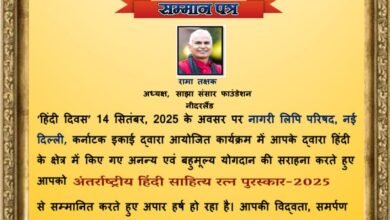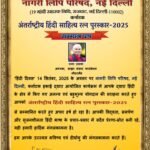कितने ही मनुष्य प्रारब्ध यानि भाग्य को प्रधान बताते हैं और कितने ही पुरुषार्थ को। वास्तव में अपने-अपने स्थान में ये दोंनो ही प्रधान हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में धर्म और मोक्ष साधन में पुरुषार्थ ही प्रधान है। इनका साधन प्रयत्न-साध्य है। अपने-आप सिद्ध होने वाले नहीं है, किन्तु अर्थ और कामना की सिद्धि में प्रारब्ध ही प्रधान है, प्रयत्न तो उस तक पहुँचने की सीढ़ी है, अन्यथा उस तक नहीं पहुँचा जा सकता।
अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्वकृत कर्म यानि प्रारब्ध और संचित भी इसमें सहायक हैं या नहीं? सो इनसे सहायता तो मिलती है किन्तु इनकी प्रधानता नहीं है। पूर्व में निष्काम भाव से किए हुए कर्म और उपासना के फलस्वरूप मनुष्य को संत-महात्माओं का संग प्राप्त होता है, किन्तु उनके मिलने पर उनके बताये गए मार्ग पर अग्रसर हो मनुष्य प्रयत्न करे तो उसका कल्याण हो जाता है। मुक्ति और भोजन-पानी कभी व्यक्ति के पास स्वत: नहीं आते। इनका आनन्द लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, कठिन श्रम करना पड़ता है। गीता में श्रीकृष्ण ने बताया है कि-
अध्यात्म से अंजान हैं, अति अज्ञ नर हरि पूजते।
दूसरों से सुन, जगत भवसिन्धु को वे लंघ्यते।।
संसार सागर को तरें, वे पार जो है मृत्यु सम।
अनभिज्ञ अरु हैं मन्द, करते साधना, श्रद्धा परम।।
अर्थात पूर्वकृत कर्म के संस्कार अच्छे होने से वे साधक के मोक्ष धाम में शामिल हो जाते हैं।। प्रारब्ध तो अपना फल देकर शान्त हो जाता है, जबकि निष्काम भाव से किए गए संचित कर्म और उपासना रुप साधन का कभी विनाश नहीं होता है। वे क्रमश: वृद्धि को प्राप्त होकर मुक्ति ही प्रदान करते हैं।
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। (गीता-2/40) अर्थात
“इस कर्म में है बीज रक्षित, नहीं फल का दोष है।” संसार में प्राणी, पदार्थ, घटना की प्राप्ति अपनी इच्छा से परे ईश्वराधीन है यानि प्रकृति के आधीन है। सभी फल भोगों को प्रारब्ध कहते हैं। विचारपूर्वक किए जाने वाले क्रियमाण कर्म का नाम प्रयत्न है। उसके तीन भेद हैं- शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुभा-शुभ कर्म। इनसे क्रमश: सुख, दु:ख और सुख-दुःख प्राप्त होते हैं।
अनिष्ट मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण: फलम्। (18/12) अर्थात
अच्छा-बुरा, मिश्रित, त्रिविध हैं कर्मफल, कर त्याग तन।
पावैं, रहे जन दूर त्यागी, कर्म कर नहिं कर्म सुन।।
किसी कर्म को मनुष्य सकाम भाव से करता है तो उसका इस लोक में पदार्थों की प्राप्ति और परलोक में स्वर्गादि की प्राप्ति रुप फल होता है।तथा निष्काम भाव से किए गए थोड़े से भी कर्तव्य-पालन का फल परमात्मा की प्राप्ति रुप मुक्ति है।स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। (गीता-2/40) अर्थात इस कर्मयोग रुप धर्म का थोड़ा-बहुत साधन जन्म-मृत्यु रुप महान भय से रक्षा कर लेता है।
रक्षित करे भव-भय से इसका, स्वल्प-साधन पोष है।।
मनुष्य कर्म करने में अधिकाँश स्वतन्त्र है, पर फल-भोगों में परतन्त्र है। देखिए-
है कर्म में अधिकार तव, फल की नहीं इच्छा करो।
हो कर्मफल का हेतु मत, अनुरक्ति अकर्म में भरो।।
कर्म करना है तुझे, वो ही तेरा अधिकार है।
फल की नहीं इच्छा करो, वही ब्रह्म को स्वीकार है।।
किन्तु मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति को भाग्य पर छोड़ देता है तो वह ईश्वर रुप अनुभव से वंचित हो जाता है। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाग्य भरोसे ईश्वर मिल गया हो। मुक्ति अपने-आप होती तो सबको मिल गई होती। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति तो शुद्ध अन्त:करण में होती है, जहाँ बच्चे और संत जैसी निर्मलता और सरलता, सहजता हो, बस! निष्काम भाव से कर्म में शुद्ध अन्त:करण फलित और विद्यमान होता है। यह सब प्रयत्न से होता है।
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को शुद्धात्मा मनुष्य कर्मयोग द्वारा पा लेता है, और कितनों ने पाया है! (गीता-4/38) अर्थात
ज्ञान सम पावन, अडिग नहिं, जगत में तुम जान लो।
समत्व बुद्धीयोग में, शुचि उर लिए, नित मान लो।।
ज्ञान प्राप्ति का दूसरा उपाय श्रीकृष्ण ने बताया है-
श्रद्धालु भक्तियुक्त जानें, तत्व से मोहि भक्तजन।
लीन मुझमें निरन्तर, मुझको भजें जग बिच स्वजन।।
मन रमा मुझमें निरन्तर, प्राण अर्पण मुझे कर।
जनाते करि भक्ति-चर्चा, मुझे जग में, हर्ष भर।।
मेरे गुणों का गान कर, वे भक्ति में सन्तुष्ट हों।
बढ़ाते पिरभाव मेरा, मुझमें रमन अरु तुष्ट हों।।
करें नित वे ध्यान मेरा, प्रेम से भजते मुझे।
योग है तत्वज्ञ का जो, रुप देता में तुझे।।
अवस्थित कर होऊँ मैं, उन हेतु करने अनुग्रय।
तम नष्ट होता तत्व ज्ञान, प्रकाश से, सुनु धनञ्जय।।
यह ईश्वर की भक्ति प्रयत्न साध्य है। जो मनुष्य ईश्वर की शरण होकर अपने ऊपर उनकी कृपा मानकर, श्रद्धा-प्रेमपूर्वक ईश्वर की भक्ति करता है, वह ईश्वर प्राप्ति रुप परम धन को ईश्वर की कृपा से पा लेता है।
अब, ज्ञान प्राप्ति का तीसरा उपाय है- तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा पुरुषों का संग और सेवा करना। ऐसा करने से भी परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में अर्जुन से श्रीकृष्ण कहते हैं- तत्व ज्ञानी पुरुष को, सेवो रहो नित प्रेम से।
निष्कपट, निश्छल तुम्हें लख, वे कहेंगे नेम से।।
तत्वज्ञ की सेवादि से, ज्ञानी करें सेवाभिवादन।
निश्छल हृदय से प्रश्न हो, वे ज्ञान दें उपदेश साधन।।
उस ज्ञान से तेरा हटेगा, मोह, चेतन रुप हो।
समदृष्टि एकीभाव, जग मुझमें, जगत मम रुप हो।।
यदि तुम्हारे पाप हैं, सबसे अधिक जग में प्रबल।
ज्ञान नौका तार दे सब अघों से, निश्चित, अटल।।
नष्ट कर देती है ईंधन को, अगिनि हो प्रज्ज्वलित।
नष्ट हों ज्ञानाग्नि में, कर कर्म अर्जुन जगत हित।।
ज्ञान सम पावन अडिग नहिं, जगत में तुम जान लो। (गीता- 4/ 34-38)
ज्ञान का प्राप्ति में जो साधन हैं, उनको भी श्रीकृष्ण ने अध्याय-13 के श्लोक- 7-11 तक बताया है-
द्वेष, इच्छा, दु:ख-सुख, नर-पिंड, तन व चेतना।
कहा है संक्षेप में, घृति विकारों सह लेखना।।
अभिमान, दंभाचरण से जो रहित, परसेवा करै।
सरल, श्रद्धा, भक्तियुत हो, क्षैम, शुचि अन्त: भरै।।
द्वेष, रागादिक, कपट से मुक्त हो, मन से परे।
इन्द्रिय व तन-मन का करे निग्रह, गुरु सेवै, डरै।।
सर्व भोगों से परे, आसक्ति तजि अरु अहम् को।
दु:ख, दोषमय देखे, जरा अरु रोग, मृत्यू, जनम को।।
धनादि, घर,परिवार स्त्री, सुतों में प्रेम हो नहिं मोह हो।
ममता रहित, समचित्त, जग प्रिय, या अप्रियजन द्रोहि हो।।
मुझ ईश में स्थित हो, एकीभाव से, कर ध्यान जो।
चिन्तन करे मम भक्त मेरा, हीन विषयी मान वो।।
विमल थल एकांतवासी, ईश लख सर्वत्र ही।
वही ज्ञानी है लखै विपरीत वो अति अज्ञ ही।।
इसी प्रकार अध्याय-18 में 50-55 श्लोक में तत्वज्ञ प्राप्ति के उपाय बताये हैं-
तन-मन-वचन पावन हो, अंतस शुद्धि पाता सिद्धि नर।
निर्बोध से जिमि ब्रह्म पाता, तत्व ज्ञानी सुत अजर।।
सेवन करे शुचि प्रेम का, एकांत, बुद्धि विशुद्ध हो।
तन व मन को जीत नर, हो मिताहारी सिद्ध हो।।
वैराग्य दृढ हो ध्यान योगी, धारणा सात्विक लहै।
ज्ञान, विषयरु, राग-द्वेषों को, नसै, उर वश रहै।।
संग्रह, अहं, बल, काम, क्रोधरु, दर्प, ममता त्याग कर।
योग्य होता, ब्रह्म एकीभाव हित वो श्रेष्ठ नर।।
ब्रह्ममय हर्षित नरात्मा, शोक-आकांक्षा रहित।
मम पराभक्ती लहै, सब भूत में समभाव रत।।
उस भक्ति से मम तत्व जाने, तत्व से जाने मुझे।
मैं मेरा पिरभाव सह हो, लीन मुझमें कहुँ तुझे।।
निष्काम हो मेर् परायण, कर्मयोगी कर्म करता।
मेरी कृपा से सनातन, अविनाशी पद वह परम लहता।।
सदाचार रुप धर्म की सिद्धि भी प्रयत्न से होती है। महर्षि मनु ने धर्म के चार लक्षण बतलाये हैं- वेद:, स्मृति:, सदाचार:, स्वस्य च प्रियमात्मन:।
एतश्चतुर्विधं प्राहु: साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम्।। अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी रुचि के अनुसार परिणाम में हितकर- यह चार प्रकार का धर्म साक्षात् लक्षण है। तथा सामान्य धर्म का स्वरुप वर्णन करते हुए मनु ने कहा है-
धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिन्द्रिय निग्रह:।
धीर्विद्या सत्यम क्रोधो, दशकं धर्म लक्षण:।।
धैर्य, क्षमा, मनोनिग्रह, चौरी न करना, तन-मन की पवित्रता, जितेन्द्रिय, सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान, सत्य वचन बोलना और अक्रोधी- ये धर्म के दस लक्षण हैं। इस प्रकार वर्णों और आश्रमोंके विशेष धर्म भी विस्तारपूर्वक मनु ने मनु स्मृति के तीसरे से छठे अध्याय तक बताये हैं। ये सभी प्रयत्न-साध्य हैं। बिना प्रयत्न के अपने-आप भाग्य से इनमें से किसी भी क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती है।
इसलिए यही सिद्ध हुआ कि अर्थ और काम अर्थात कामना की प्राप्ति में तो प्रारब्ध की प्रधानता है तथा धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में प्रयत्न की प्रधानता है। नल-दमयन्ती, दिलिप, रघु, पाँचों पाण्डव (श्रीकृष्ण के मित्र और रिश्तेदार), नरसी, मोरध्वज, रावण, वाणासुर, परशुराम, जमदग्नि, श्रीराम-सीता एवं श्रीकृष्ण और भी अनेक परम, महान पुरुषों के उदाहरण हैं जो नियति और भाग्य के आगे कुछ भी न कर पाये। वहाँ परमात्मा की भी नहीं चली। प्रकृति के अधीन ईश्वर भी है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। को करि तर्क बढ़ावहि शाखा।। जय श्रीराम! जय श्रीकृष्ण! जय सीता-राधा!!
आलेख रचनाकार एवं संकलन-
पं० जुगल किशोर त्रिपाठी (साहित्यकार)
बम्हौरी, मऊरानीपुर, झाँसी