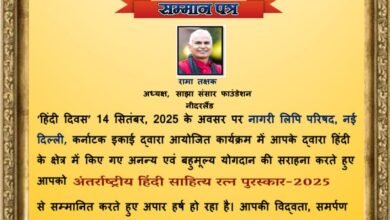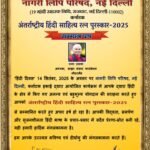श्लोक:-
मध्यत आद त ईदं न दोषाय वर्तते, परंतु येन सार्थं वित्तं द्राक्ष्यं जातम्।
— ऋग्वेद – पुस्तक १०, सूक्त ३४
“मैंने अपनी संपत्ति जुआ खेल में गंवाई, इसका पछतावा आज भी है।”
भावपल्लवन
यह श्लोक ऋग्वेद के दसवें खंड के 34वें सूक्त से लिया गया है, जिसे “अक्षसूक्त” कहा जाता है। यह ऋषि कक्षीवत् गामायन द्वारा रचित है। इसमें जुए (अक्ष) को केवल एक खेल न मानकर, उसे इंसान की कमजोरियों, बिना सोच-समझ के आकर्षणों और परिवार व समाज को तोड़ने वाली प्रवृत्तियों का प्रतीक बताया गया है। ऋग्वेद में “अक्ष” शब्द जुआ खेलने के पासों के लिए आता है, जो यहाँ मोह-माया और विनाशकारी प्रवृत्तियों का संकेत बन जाता है। यह सूक्त एक जुआरी की आत्मस्वीकृति के माध्यम से समाज को चेतावनी देता है और पश्चाताप की भावना को दर्शाता है।
संधिविग्रह:
मध्यत् + आत् + तत् + ईदं + न + दोषाय + वर्तते,
परंतु + येन + सार्थम् + वित्तम् + द्राक्ष्यम् + जातम्।
अर्थ:
“जब मैंने प्रारंभ में जुए का आरंभ किया, तब यह मुझे दोषयुक्त नहीं प्रतीत हुआ; परंतु जिस क्षण मैंने देखा कि इसके कारण मेरा संचित धन और सार्थक जीवन लुट गया — वही क्षण मेरे पतन की शुरुआत बन गया।”
यह श्लोक केवल भौतिक हानि की नहीं, बल्कि आत्मिक क्षरण की गाथा है, जो आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक और चेतनादायक है।
शब्दार्थ
मध्यत — मध्य में, बीच में (जुए के बीच)
आद — आरम्भ से, प्रारंभ में
त — वह (यह क्रिया/कार्य)
ईदं — यह (कार्य)
न दोषाय — दोष का कारण नहीं
वर्तते — होता है, होता रहा है
परंतु — किन्तु, परन्तु
येन — जिससे
सार्थम् — सामान सहित, संपत्ति सहित
वित्तम् — धन, संपत्ति
द्राक्ष्यम् — जो देखा गया, प्राप्त हुआ (या देखा जाएगा)
जातम् — उत्पन्न हुआ, हुआ
(“जुए के प्रारंभ में यह दोष नहीं माना जाता, किन्तु जिससे संपत्ति सहित धन की हानि हुई, वह (कार्य) दोषपूर्ण बन गया।”)
इस श्लोक में एक जुआरी की गहन आत्मस्वीकृति प्रकट होती है, जिसमें वह स्वीकार करता है कि जब उसने जुए की शुरुआत की, तब यह कृत्य उसे दोषयुक्त प्रतीत नहीं हुआ — अर्थात् उस समय उसकी विवेक-बुद्धि मोहवश मलिन हो चुकी थी। “मध्यत्” शब्द यह इंगित करता है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्रायः किसी भी विकृति या अधःपतन को दोष नहीं मानता; वह उसे आकर्षण, आनंद अथवा केवल एक खेल का साधन मान बैठता है। परंतु जब “वित्तं द्राक्ष्यं जातम्” — अर्थात् संपूर्ण धन, श्रम और जीवन की सार्थकता को अपनी आँखों के सामने नष्ट होता हुआ देखता है, तभी उसे अपनी भूल का गहन बोध होता है। यहाँ “दोषाय वर्तते” वाक्यांश में ‘दोष’ की काल-सापेक्ष अनुभूति निहित है। प्रारंभ में दोष का अदृश्य रहना और कालांतर में उसका प्रत्यक्ष रूप में उद्घाटित होना। यह श्लोक केवल धन की हानि की बात नहीं करता, बल्कि उस आत्मिक गिरावट, सामाजिक अपयश और पश्चाताप की तीव्र पीड़ा को दर्शाता है, जो जुए जैसे व्यसन के पीछे छिपी होती है। यह भाव आज भी हर उस मनुष्य के लिए एक दर्पण है, जो क्षणिक सुख में स्थायी मूल्यों को भुला बैठता है।
इस श्लोक में निहित भाव मानव-जीवन के उस गहन नैतिक द्वंद्व को उद्घाटित करता है, जहाँ प्रवृत्ति (आकर्षण, लालसा, सुख की इच्छा) और विवेक (नैतिक discernment) के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। जुआ, जो आरंभ में एक सामान्य खेल या त्वरित धनार्जन का साधन प्रतीत होता है, क्रमशः मनुष्य को ऐसे मार्ग पर ले जाता है, जहाँ अनुचित उपायों से प्राप्त द्रव्य अंततः उसकी चेतना को कलुषित कर देता है। “वित्तं द्राक्ष्यं जातम्” केवल धन की हानि का संकेत नहीं करता, अपितु आत्मसम्मान, पारिवारिक संबंधों एवं जीवन की मूल अर्थवत्ता के क्षरण की ओर भी संकेत करता है। इसी बिंदु पर आत्मग्लानि का जन्म होता है। जब मनुष्य अपनी भूल को समझता है, किंतु तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। यह पश्चाताप केवल अतीत की भूल नहीं, बल्कि उसकी नैतिक चेतना का पुनर्जागरण है, जो उसे अपनी ही प्रवृत्तियों पर आत्मचिंतन और आत्मपरीक्षण हेतु विवश करता है। यही आंतरिक संघर्ष वैदिक वाणी में अत्यंत संवेदनशीलता और मार्मिकता के साथ प्रकट हुआ है, जो आज भी प्रत्येक युग के मनुष्य के लिए दर्पण और दिशा प्रदान करता है।
वैदिक दृष्टिकोण से जुआ (अक्ष) केवल एक खेल नहीं, अपितु एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे मोह, प्रमाद और अधर्म का स्रोत माना गया है। ऋग्वेद के द्यूतसूक्त (१०.३४) में जहाँ एक जुआरी की आत्मस्वीकृति के माध्यम से चेतावनी दी गई है, वहीं अन्य मन्त्रों में ‘अक्ष’ विषयक उल्लेख प्रतिबंधात्मक और निवारणात्मक रूप में प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद (३०.१८) में द्यूत को स्पष्टतः त्याज्य घोषित किया गया है— “अक्षं दूत्यं परिवर्जयेत्” — अर्थात् जुए और पासों का परित्याग करना चाहिए। वैदिक जीवन-दृष्टि में सत्कर्म, श्रम और धर्मपालन को ही धन एवं यश का वास्तविक स्रोत माना गया है, न कि अनिश्चित, प्रमादी और भाग्याश्रित उपायों को। जुआ इस दृष्टि से पुरुषार्थविहीन संपत्ति की कामना का प्रतीक है, जो व्यक्ति को कर्म-पथ से विचलित करता है। अतः वेदों में जहाँ एक ओर जुए की नैतिक हानि को उकेरा गया है, वहीं यह भी सिखाया गया है कि परिश्रम, संयम और धर्मनिष्ठा से अर्जित द्रव्य ही जीवन को स्थायित्व और सम्मान प्रदान करता है। इस प्रकार, वैदिक वाङ्मय में जुए को केवल वर्जनीय ही नहीं, अपितु आत्मिक पतन की प्रक्रिया के रूप में भी निरूपित किया गया है।
आधुनिक सन्दर्भों में जुए का पुनर्पाठ करें तो यह स्पष्ट होता है कि आज जुआ परंपरागत पासों और चौपड़ की सीमाओं से निकलकर ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाज़ी, फैंटेसी गेम्स, क्रिप्टो-सट्टा और डिजिटल कैसिनो जैसे अनेक आधुनिक रूपों में परिवर्तित हो चुका है। ये सभी स्वरूप अत्यधिक आकर्षक, छलावरणयुक्त और सर्वसुलभ बन गए हैं, जो व्यक्ति को त्वरित लाभ के मोहजाल में फँसाते हैं। इस मोह में फँसा मनुष्य बिना श्रम के धन प्राप्ति की आकांक्षा में धीरे-धीरे नैतिक पतन, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट और सामाजिक अलगाव की ओर अग्रसर होता जाता है। परिवारों में कलह, विश्वास का विघटन और सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास इसके सामान्य दुष्परिणाम बनते जा रहे हैं।
यह आधुनिक जुआ, यद्यपि तकनीकी आवरण में लिपटा हुआ है, परंतु इसकी जड़ वही पुरातन प्रवृत्तिगत मोह है, जिसे वैदिक ऋषियों ने “द्यूत” कहकर त्याज्य घोषित किया था। आज आवश्यकता है उस वैदिक चेतना के पुनर्जागरण की, जो सत्कर्म, श्रम और विवेक के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है, ताकि आधुनिक समाज मूल्यहीन त्वरित लाभ की इस अंध दौड़ से बाहर निकलकर धर्म, संयम और विवेकपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सके।
वैदिक वाङ्मय केवल निषेधात्मक निर्देश नहीं देता, अपितु संयम, विवेक और तपश्चर्या के माध्यम से आत्मशुद्धि की उच्च प्रेरणा भी प्रदान करता है। जुए जैसी प्रवृत्तियाँ तब प्रकट होती हैं, जब मनुष्य इंद्रियभोग, त्वरित सुख और परिश्रमविहीन संपत्ति की आकांक्षा में डूब जाता है। वैदिक संकेत बताते हैं कि इन विकारों का मूल नियंत्रण अंतर्बोध और तप एवं साधना में निहित है। यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद में द्यूत का स्पष्ट निषेध करते हुए सत्कर्म, यज्ञ, स्वाध्याय और तप को विवेक-जागरण के साधन रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। संयम की यह साधना केवल बाह्य आचरण के नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि चित्त की वृत्तियों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य मूल्यनिष्ठ जीवन की दिशा में उन्नत होता है। इस दृष्टि से वैदिक मार्ग केवल दमन का नहीं, अपितु उद्धार का पथ है, जहाँ आत्मशुद्धि के माध्यम से मनुष्य स्वयं अपने दोषों को पहचानकर, उनके परित्याग में शक्ति प्राप्त करता है और धर्म-सम्मत, संतुलित तथा सार्थक जीवन की स्थापना करता है।
ऋग्वेद का यह श्लोक केवल अतीत की कोई कथा नहीं, अपितु आधुनिक मानव के लिए एक दर्पण है, जो उसे आत्मनिरीक्षण और नैतिक जागरूकता को जगाता है। यह श्लोक सिखाता है कि जब मनुष्य क्षणिक सुखों की ललक में विवेकहीन होकर अपने श्रम, संबंधों और सम्मान को दाँव पर लगा देता है, तब वह अंततः गंभीर आत्मग्लानि और अर्थहीनता की ग्रंथि में जकड़ा हुआ हो जाता है। यह पश्चाताप केवल निजी नहीं होता, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संतुलन को भी विक्षिप्त कर देता है। वैदिक ज्ञान मानव को संयम, श्रम, सत्कर्म और विवेक का पथ प्रदर्शित करता है। हमें आत्मचेतना की दिशा में अग्रसर करता है। यह श्लोक स्पष्ट संदेश देता है कि सच्चा लाभ वही है, जो धर्ममय हो, श्रमसिद्ध हो और विवेकयुक्त हो। इस प्रकार, वैदिक वाणी के माध्यम से ज्ञान और आत्मचेतना का संगम ही आज की दिशाहीनता और अधोगति से मुक्ति का मार्ग है। जहाँ मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे आलोकित जीवन में रूपांतरित कर सकता है।
ऋग्वेद के अक्षसूक्त का यह श्लोक जुए के माध्यम से मनुष्य की आत्मविस्मृति, नैतिक पतन और पश्चाताप की गहन अनुभूति को प्रकट करता है। प्रारंभ में हानिरहित प्रतीत होने वाला जुआ अंततः व्यक्ति के श्रम, संबंध और आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है, जिससे वह आत्मग्लानि और सामाजिक विघटन से घिर जाता है। वैदिक वाङ्मय इस प्रवृत्ति को केवल निषिद्ध ही नहीं ठहराता, बल्कि संयम, श्रम और विवेक के मार्ग पर चलकर आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। आधुनिक तकनीकी युग में जुए के नए स्वरूप जैसे- ऑनलाइन सट्टा, फैंटेसी गेम्स आदि उसी पुरातन मोह का रूप हैं, जिसे वैदिक ऋषियों ने ‘द्यूत’ कहकर त्यागने योग्य बताया था। इस श्लोक में निहित चेतना आज के समाज के लिए दर्पण बनकर आत्मावलोकन और नैतिक जागरण की ओर प्रेरित करती है, जहाँ मनुष्य धर्म, संयम और विवेकपूर्ण जीवन के मार्ग पर लौटकर स्थायी सुख और संतुलन की ओर अग्रसर हो सकता है।
अंततः, ऋग्वेद का यह श्लोक उस वैदिक चेतना का प्रतीक है जो केवल मार्गदर्शन नहीं, आत्मग्लानि के अंधकार से आत्मप्रकाश की ओर ले जाने वाली प्रकाश-पंक्ति है, जहाँ मनुष्य अपने ही अविवेकजन्य कर्मों से उबरकर धर्म, श्रम और संयम के आलोक में जीवन का पुनर्निर्माण कर सकता है।
योगेश गहतोड़ी