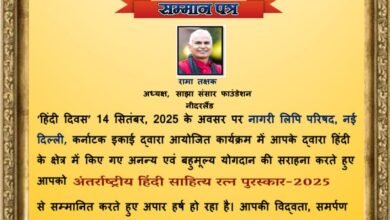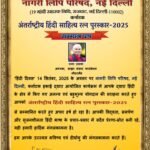श्लोक:-
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥”
(बृहदारण्यक उपनिषद् एवं मन्त्र पुष्पाञ्जलि)
“अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी शुभ दृष्टि से युक्त हों, कोई भी दुःखी न हो।”
आलेख- योगेश गहतोड़ी
यह शांति मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद् से लिया गया है, जो यजुर्वेद की ज्ञान परंपरा से जुड़ा है और समय के साथ यह मंत्र पुष्पांजलि का हिस्सा भी बन गया। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए एक गहरी करुणा है। इसका संदेश यह है कि सच्ची शांति तब ही संभव है जब हर जीव सुखी, स्वस्थ, शुभ दृष्टि से युक्त और दुःख-मुक्त हो। यह मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारी चिंता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें समग्र समाज और सृष्टि का भला सोचना चाहिए। यह करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि हमारे जीवन का तरीका होना चाहिए, जिसमें हम हर जीव के लिए मंगलकामना करते हैं। वैदिक संस्कृति में धर्म, करुणा और समाज की भलाई एक साथ जुड़े हुए हैं, और यही इस मंत्र का मूल संदेश है।
शब्दार्थ
सर्वे सभी / सब लोग
भवन्तु हों / हो जाएँ
सुखिनः सुखी / आनंदित
सर्वे सभी
सन्तु रहें / बने रहें
निरामयाः निरोग / रोगों से मुक्त
सर्वे सभी
भद्राणि शुभ / कल्याणकारी बातें
पश्यन्तु देखें / अनुभव करें
मा मत / नहीं
कश्चित् कोई भी व्यक्ति
दुःख दुःख / पीड़ा
भाग्भवेत् भागी हो / हिस्सा बने
यह श्लोक केवल एक याचना नहीं, वरन् एक समष्टिगत संकल्प है, जो हर जीव के कल्याण की भावना को उद्घाटित करता है।
“सर्वे भवन्तु सुखिनः” — इस वैदिक शांति मंत्र में निहित ‘सुख’ की अवधारणा इन्द्रियजन्य या भौतिक सुख से कहीं आगे आत्मिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर व्यापक है। पहला स्तर आत्मिक तृप्ति का है, जहाँ व्यक्ति अपने अंतर्मन में शांति, संतुलन और ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति करता है। दूसरा स्तर सामाजिक समरसता का है, जहाँ सुख केवल निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि पारस्परिक सहयोग, सौहार्द और समानता पर आधारित होता है। तीसरा स्तर नैतिक संतोष का है, जहाँ धर्मयुक्त आचरण और कर्तव्यपरायण जीवन से उत्पन्न आंतरिक संतोष सुख का मूल बनता है और चौथा स्तर समष्टि के साथ तादात्म्य का है, जिसमें सुख स्व-केंद्रित नहीं, बल्कि ‘सर्वे’ की मंगलकामना से जुड़ा होता है। वैदिक संस्कृति इस श्लोक के माध्यम से यह उद्घोष करती है कि यदि समाज का कोई एक प्राणी भी दुःख में है, तो किसी एक का सुख पूर्ण नहीं हो सकता। अतः यह मंत्र सुख की ऐसी सार्वभौमिक परिकल्पना है, जहाँ ‘स्व’ का विस्तार ‘सर्व’ में होता है और यही वैदिक करुणा का सार है।
“सर्वे सन्तु निरामयाः” — इस शांति मंत्र का ‘निरामय’ शब्द केवल रोग-मुक्ति का बोध नहीं कराता, बल्कि वैदिक दृष्टिकोण में समग्र स्वास्थ्य की बहुस्तरीय भावना को उद्घाटित करता है। इसमें पहला स्तर शारीरिक आरोग्यता का है, जहाँ शरीर स्वस्थ, संतुलित और दोष-मुक्त हो। दूसरा स्तर प्राणमय कोष की ऊर्जा का है, जो जीवन की क्रियाशीलता और उत्साह का स्रोत है। तीसरा स्तर मनोमय कोष की स्थिरता और मानसिक संतुलन का है, जो चिंताओं, कामनाओं और भय से मुक्त मन के रूप में सुख का आधार बनता है। चौथा स्तर विज्ञानमय और आनंदमय कोष की विवेकपूर्ण पूर्णता का है, जहाँ ज्ञान, तत्त्वबोध और आत्मानंद मिलकर रोगरहित जीवन का वास्तविक आधार बनते हैं। वैदिक संस्कृति में ‘निरामयता’ औषधियों तक सीमित नहीं, बल्कि सम्यक् आहार, पवित्र विचार और संयमित व्यवहार से उपजी जीवनशैली का प्रतिफल है। यह मंत्र इसलिए केवल शरीर की नहीं, सम्पूर्ण मानव-सत्ता की शुद्धि और संतुलन की मंगलकामना करता है, जिससे समाज में रोग नहीं, ऋतु-सम्मत जीवन और ऋत-चिंतन का सामंजस्य स्थापित हो।
“सर्वे भद्राणि पश्यन्तु” — इस वैदिक शांति मंत्र में ‘भद्र’ का आशय केवल बाह्य शुभता या सौंदर्य से नहीं, बल्कि चार स्तरीय गहराई में छिपे हुए जीवन के अंत:सौंदर्य से है। प्रथम स्तर पर यह इन्द्रियजन्य दृष्टि को संयमित करता है, जिससे हम बाह्य जगत में सौंदर्य, सुव्यवस्था और शांति है। द्वितीय स्तर बुद्धिदृष्टि का है, जहाँ विवेक, तर्क और न्याय की दृष्टि से जीवन को समझने की क्षमता विकसित होती है। तृतीय स्तर भावदृष्टि का है, जो करुणा, प्रेम और समरसता की दृष्टि से हर प्राणी में शुभता को देखने की शक्ति प्रदान करता है। चतुर्थ और गहनतम स्तर आत्मदृष्टि का है, जिसमें हम जगत को नहीं, स्वयं को शुभ-स्वरूप में देखते हैं और उसी दृष्टि से समस्त सृष्टि का साक्षात्कार करते हैं। यह श्लोक समाज में भद्र-दृष्टि के उस जागरण का आह्वान करता है, जिससे वैमनस्य, कलुषता और हिंसा का अंधकार स्वतः दूर होता है और सह-अस्तित्व, सहिष्णुता तथा सद्भाव की ज्योति स्वतः प्रज्वलित होती है। यह दृष्टिकोण न केवल मानवीय व्यवहार को संस्कारित करता है, बल्कि आत्मा को आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर भी ले जाता है।
“मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्” — इस मंत्र की यह अंतिम पंक्ति केवल दुःख के अभाव की निष्क्रिय कामना नहीं, अपितु एक गहन सामाजिक और आत्मिक संकल्प है, जिसमें करुणा को चार स्तरीय क्रियाशीलता में रूपांतरित किया गया है। प्रथम स्तर पर यह मानसिक संवेदना का है, जहाँ हम दूसरों के दुःख को केवल ‘देखते’ नहीं, अनुभव करते हैं। द्वितीय स्तर पर यह नैतिक उत्तरदायित्व का भाव जगाता है, जहाँ दुःख को देखकर मन हटता नहीं, अपितु सहायता के लिए आगे बढ़ता है। तृतीय स्तर इसका सामाजिक समावेशन है, जहाँ करुणा सेवा, दान, न्याय और समानता के रूप में कार्य करते हुए दुःखी जीव को केवल सांत्वना नहीं, सहयोग और सशक्तिकरण भी देती है। चतुर्थ और अंतिम स्तर आध्यात्मिक सहभागिता का है, जहाँ हम प्रत्येक दुःखी जीव को आत्मस्वरूप मानकर उसके कष्ट को दूर करने को अपना कर्तव्य समझते हैं। इस प्रकार यह मंत्र केवल प्रार्थना की पुकार नहीं, बल्कि प्रयत्न का पथ है। जिसमें वैदिक करुणा निष्क्रिय भावना नहीं होती है, बल्कि वह सक्रिय, कर्मशील और सहभागी चेतना के रूप में समस्त समाज के दुःख-निवारण का संकल्प करती है।
“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥” यह शांति मंत्र वैदिक दर्शन की उस समष्टि-दृष्टि को दिखाता है, जिसमें इंसान की चार सबसे जरूरी कामनाएं — सुरक्षा, सम्मान, सुख और स्वतंत्रता शामिल हैं। यह कामनाएं सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और आत्मा के स्तर पर भी पूरी होनी चाहिए। यह श्लोक जिस ‘सुख’ की बात करता है, वह केवल इन्द्रियों की तृप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन से जुड़ा होता है। इसमें ‘धर्म’ का मतलब केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और जिम्मेदारी से भरा जीवन होता है। ‘अर्थ’ का सही और शुभ उपयोग करने की प्रेरणा यह मंत्र देता है, ताकि हम लोभ और हिंसा से मुक्त होकर विवेक और शुभ दृष्टि से जीवन को देखें। अंत में, कोई भी दुःखी न हों और सभी सुखी होते हुए मुक्त हो जाएँ, तो वही ‘मोक्ष’ की स्थिति बनती है। जहाँ आत्मा बंधनों से आज़ाद होकर अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होती है। इस तरह, यह मंत्र केवल अपने सुख की प्रार्थना नहीं है, बल्कि पूरे समाज और सृष्टि के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के संतुलन के साथ संपूर्ण कल्याण की कामना करता है।
“वसुधैव कुटुम्बकम्” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः…” — यह दोनों वैदिक सूत्र एक ही आध्यात्मिक तंतु में गुँथे हुए हैं, जहाँ समस्त विश्व को एक परिवार मानते हुए, उसके प्रत्येक सदस्य के सुख, स्वास्थ्य, शुभदृष्टि और दुःखमुक्ति की मंगलकामना की जाती है। “वसुधैव कुटुम्बकम्” उस व्यापक भावभूमि की स्थापना करता है जिसमें समस्त जीव-जगत, मानवता, प्रकृति और संस्कृति एक सूत्र में बँधे हुए हैं और “सर्वे भवन्तु सुखिनः…” उसी भावभूमि पर आधारित समर्पित प्रार्थना है — जो केवल विचार नहीं, कर्मशील करुणा का आह्वान करती है। यह श्लोक “स्व” से “सर्व” की यात्रा को धर्म, स्वास्थ्य, विवेक और मोक्ष की चार सीढ़ियों में पूर्ण करता है, जहाँ हर जीवन की भलाई हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। इसलिए इन दोनों सूत्रों का संबंध केवल वैचारिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और आध्यात्मिक भी है। एक वैश्विक व्यवस्था का सपना, जो संवेदना, समता और सह-अस्तित्व पर आधारित हो, जहाँ किसी को भी दुःख का भागी नहीं होना पड़े। यही वैदिक धर्म की करुणा में संलग्न कर्म समष्टि-दृष्टि है।
आज जब सारा संसार, युद्धों की विभीषिका से भयभीत है, मानसिक रोग असाधारण गति से बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका है और मानव के भीतर की आत्मीयता क्षीण होती जा रही है — तब “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥” जैसा शांति मंत्र एक वैदिक प्रकाशस्तंभ की भाँति सामने आता है। यह मंत्र हमें स्मरण कराता है कि आज की जटिल समस्याओं का समाधान केवल विज्ञान या तकनीकी प्रगति में नहीं, बल्कि करुणा, सह-अस्तित्व और समष्टि कल्याण की वैदिक चेतना में है। यह उद्घोष करता है कि मानवता को तकनीक नहीं, करुणा बचाएगी। वह करुणा जो दूसरों के सुख को अपना सुख माने, जो रोग, दुःख और विषमता को केवल आँकड़ों में नहीं, अपने भीतर की पीड़ा में अनुभव करे और जो समस्त विश्व को परिवार मानकर, हर प्राणी के कल्याण हेतु प्रयत्नशील हो। यह श्लोक आज की विकृत होती संवेदनाओं के बीच एक संतुलनकारी, आत्मगामी और शाश्वत मार्गदर्शक बनकर खड़ा है।
इस शांति मंत्र का महत्व केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन के लिए एक गहरी और व्यापक दिशा छुपी है। ज़रूरी है कि इसे व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए। जैसे- विद्यालयों में बच्चों को बचपन से करुणा, समानता और सह-अस्तित्व का संस्कार देना। राजनीति और नीति-निर्माण में यह केवल आदर्श न रहकर जनकल्याण की सक्रिय प्रेरणा बने। समाज में यह सेवा, सहयोग और सद्भाव की भावना फैलाए, जो सभी भेदों से ऊपर उठकर मानवता को एक सूत्र में बाँधती है। जब यह मंत्र हमारे विचार, योजनाओं और कार्यों का हिस्सा बनता है, तब यह सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन जाता है।
“सर्वे भवन्तु सुखिनः…” यह शांति मंत्र केवल बोलने भर की प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक जिम्मेदारी है। यह हमें सिखाता है कि समाज तभी सुंदर बन सकता है जब हम सबके लिए भलाई सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी चाहें। तभी यह मंत्र हमें एक ऐसी नई सोच की ओर ले जाता है, जहाँ हर व्यक्ति के जीवन में करुणा, समानता और समझदारी का बीज अंकुरित होता है। इसमें सुरक्षा का अर्थ है — भय, भूख, बीमारी और भेदभाव से मुक्ति। सम्मान का अर्थ है — हर व्यक्ति को उसकी पहचान और गरिमा के साथ अपनाना। सुख का मतलब — केवल अपनी नहीं, सभी की भलाई और संतुष्टि की भावना और स्वतंत्रता का आशय है — दुःख, अन्याय और बंधनों से पूर्ण मुक्ति। एक ऐसा समाज जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित, सुखी और स्वतंत्र हो; यही इस मंत्र का सच्चा संदेश है।
आलेख साभार संकलन-
पं० जुगल किशोर त्रिपाठी (साहित्यकार)
बम्हौरी, मऊरानीपुर, झाँसी (उ०प्र०)