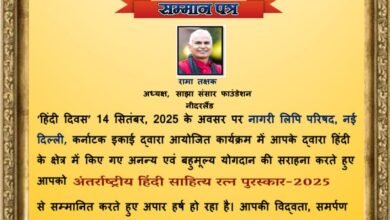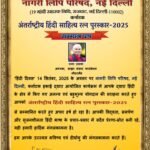(स्वरचित आलेख)
प्रस्तावना
समाज एक जीवंत, गतिशील और परस्पर जुड़ी हुई संरचना है, जिसका वास्तविक स्वरूप केवल इमारतों, सड़कों या संस्थानों जैसे भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि उसमें निहित मानवीय मूल्य, संबंध, संवेदनाएं और आदर्शों से निर्मित होता है। जब समाज में नैतिकता, समता, न्याय और सहयोग की भावना बनी रहती है, तब वह संतुलित रूप से प्रगति करता है। किंतु जब उसमें लालच, हिंसा, भेदभाव, अन्याय और सांस्कृतिक विघटन जैसे विघातक तत्व प्रवेश करते हैं, तो उसका संतुलन डगमगाने लगता है। ऐसे समय में समाज को केवल बाह्य सुधारों की नहीं, बल्कि उसके मूल्यों के स्तर पर गहन मरम्मत, पुनर्निर्माण और सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। इस सतत, उत्तरदायी और संवेदनशील प्रक्रिया को ही ‘समाजरक्षण’ कहा जाता है।
‘समाजरक्षण’ शब्द ‘समाज’ और ‘रक्षण’ — इन दो तत्वों के समन्वय से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है समाज की रक्षा, संरक्षण, पोषण और सतत सुधार। यह केवल किसी आपदा या संकट से समाज की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे नैतिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करता है। दार्शनिक दृष्टि से यह एक उच्चतर सामाजिक चेतना है, जिसमें सत्य, करुणा, न्याय, समता और सह-अस्तित्व जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक पुनर्रचना की परिकल्पना की जाती है। यह प्रक्रिया समाज को आत्मदर्शन और आत्मसंशोधन के मार्ग पर प्रेरित करते हुए समष्टि-कल्याण की दिशा में अग्रसर करने का सशक्त माध्यम बनती है।
वर्तमान युग में, जहाँ आधुनिकता, उपभोक्तावाद और तकनीकी उन्नति ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं इससे जुड़े भौतिकवाद, आत्मकेन्द्रित सोच और नैतिक विचलन ने समाज को विभाजित और दिशाहीन कर दिया है। ऐसे परिवेश में ‘समाजरक्षण’ केवल संकटों से रक्षा का उपाय नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन, सहभागिता और उत्तरदायित्व की पुनःस्थापना हेतु एक सकारात्मक पुनर्संरचना की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल दोषों को दूर करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समरस, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना है, जो न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी और नैतिक मार्ग प्रशस्त कर सके।
1. धार्मिक एवं आध्यात्मिक समाजरक्षण
वैदिक धर्म की नींव ऋत (प्राकृतिक नियम), सत्य और धर्म जैसे मूल सिद्धांतों पर रखी गई थी, जिनका उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और जिम्मेदारी के साथ जीवन यापन करे। वैदिक काल की वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रायः गलत समझा जाता है, जबकि वास्तविक रूप में यह जन्म पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, गुण और स्वभाव पर आधारित थी। इसका आशय था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और प्रकृति के अनुसार दायित्व सौंपे जाएँ, ताकि समाज में संतुलन बना रहे और सभी जन समाज-कल्याण में सहभागी बन सकें। धर्म भी केवल पूजा-पद्धति या रीति-रिवाजों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य, अनुशासन, करुणा और संयम के पालन की एक समग्र नीति थी। ‘धारयति इति धर्मः’ — अर्थात जो जीवन, समाज और सम्पूर्ण सृष्टि को धारण करे — वही धर्म है। इस प्रकार, धर्म को समाज को नैतिक, उत्तरदायी और संतुलित बनाए रखने वाली आधारशिला के रूप में स्वीकार किया गया।
भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास में संतों और सुधारकों ने समाजरक्षण की भावना को सुदृढ़ किया है। संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और रूढ़ियों का साहसपूर्वक विरोध किया और जनमानस को आत्मबोध, प्रेम, समानता तथा सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इन संतों ने धर्म को केवल कर्मकांडों तक सीमित न रखकर उसे मानवता, करुणा और समर्पण से जोड़ा। आज के समय में, जब धर्म के नाम पर संकीर्णता और कट्टरता बढ़ रही है, तब इन संतों का समावेशी और उदात्त संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। यदि हम सभी धर्मों के मूल तत्व — प्रेम, दया और मानवता को आत्मसात करें, तो मतभेदों के बावजूद एक समरस, समावेशी और एकजुट समाज का निर्माण संभव है। यही सच्चे अर्थों में धार्मिक समाजरक्षण है।
2. शैक्षिक समाजरक्षण
शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, क्योंकि यह व्यक्ति को केवल ज्ञान ही नहीं प्रदान करती, बल्कि उसे सोचने-समझने की शक्ति, उत्तरदायित्व का भाव और सामाजिक चेतना भी देती है। जब कोई समाज जागरूक, विवेकशील और संवेदनशील नागरिकों से निर्मित होता है, तभी वह सशक्त और संतुलित रूप में विकसित हो सकता है। वैदिक सूत्र ‘सा विद्या या विमुक्तये’ का अभिप्राय जो मनुष्य को अज्ञान, भय, रूढ़ियों और भेदभाव से मुक्त करे वही सच्ची शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियाँ अर्जित करना या रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को एक अच्छा मानव बनाए, उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव विकसित करे। यही शिक्षा समाजरक्षण की मूल भूमि तैयार करती है।
एक अच्छे समाज की नींव चरित्र निर्माण, नैतिकता और सबको साथ लेकर चलने वाली समावेशी सोच पर आधारित होती है। यदि विद्यालय और महाविद्यालय केवल बुद्धि को नहीं, बल्कि हृदय को भी शिक्षित करें, तो एक न्यायपूर्ण और समरस समाज की स्थापना संभव है। जो व्यक्ति शिक्षित तो हो, परंतु उसके भीतर चरित्र न हो, वह समाज के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। आज के समय में शिक्षा में तकनीकी नवाचार के साथ-साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक विविधताओं की समझ को भी समान रूप से महत्व देना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक वर्ग और समुदाय को समान अवसर मिल सकें। इसमें शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल विषयों का ज्ञाता नहीं, बल्कि भावी समाज का निर्माता होता है। यदि हमारे पाठ्यक्रमों में करुणा, नागरिकता, नैतिकता और जीवन-कौशल को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर दिया जाए, तो हम ऐसा समाज बना सकते हैं जो न केवल आत्मनिर्भर और उत्तरदायी हो, बल्कि परस्पर सहयोग और सह-अस्तित्व के आदर्शों पर भी दृढ़तापूर्वक स्थापित हो। यही सच्चे अर्थों में शैक्षिक समाजरक्षण की परिभाषा है।
3. राजनीतिक समाजरक्षण
राजनीति किसी समाज का दर्पण होती है। यदि यह दर्पण स्वच्छ और सत्यनिष्ठ हो, तो समाज की दिशा भी सही रहती है; परंतु जब राजनीति भ्रष्टाचार और स्वार्थ से ग्रसित हो जाती है, तब पूरा समाज दिशाहीन होने लगता है। राजनीति का मूल उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनसेवा और जनकल्याण होना चाहिए। जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है, अपने सभी निर्णयों में पारदर्शिता रखती है और नेताओं में उत्तरदायित्व का भाव होता है, तब समाज में विश्वास, अनुशासन और स्थिरता उत्पन्न होती है। समाज की रक्षा और सुधार के लिए ऐसी राजनीति की आवश्यकता है, जो स्वार्थ नहीं, देशहित की सोच रखे और सेवा को ही अपना सर्वोच्च धर्म माने। यही राजनीति समाजरक्षण की एक सशक्त और अनिवार्य कड़ी बन सकती है।
भारत का संविधान समाजरक्षण की एक सुदृढ़ और मूलभूत आधारशिला है। यह हमें समानता, सम्मान और न्याय जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें जहाँ वंचितों, गरीबों और पिछड़े वर्गों को सशक्त किया गया है, वहीं समृद्ध और सक्षम नागरिकों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध भी कराया गया है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि नागरिक केवल मतदान तक ही सीमित न रहें, बल्कि शासन की नीतियों में सक्रिय भागीदारी करें, सजग रहें और अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझें। जब नागरिक सचेत होते हैं, तब राजनीति भी उत्तरदायी और संवेदनशील बनती है। किंतु यदि राजनीति से नैतिकता और सेवा-भाव समाप्त हो जाए, तो समाज में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पनपने लगती है। अतः आज आवश्यकता है कि राजनीति को पुनः ईमानदारी, पारदर्शिता और जनकल्याण के मार्ग पर लौटाया जाए — यही राजनीतिक समाजरक्षण की सच्ची और आवश्यक दिशा है।
4. आर्थिक समाजरक्षण
समाज की स्थिरता और समरसता केवल अच्छे संस्कारों या नैतिक मूल्यों पर ही आधारित नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक न्यायसंगत और संतुलित आर्थिक व्यवस्था भी अनिवार्य होती है। यदि समाज में कुछ ही लोगों के पास अधिकांश संसाधन और धन एकत्र हो जाएँ, तो वंचित वर्ग जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रह जाता है। इसका परिणाम असंतोष, संघर्ष और सामाजिक भेदभाव के रूप में सामने आता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हों और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे समाज में संतुलन और सहयोग बना रहे। आर्थिक समाजरक्षण का अभिप्राय है — ऐसी नीतियाँ और व्यवस्थाएँ निर्मित करना, जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करें और विकास को मात्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रखते हुए मानव कल्याण और सामाजिक समरसता की दिशा में ले जाएँ।
इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे— मेहनतकश लोगों को गरिमापूर्ण सम्मान देना, छोटे एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपाय करना। गरीबी केवल आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं होती, बल्कि यह आत्मसम्मान, सुरक्षा और अवसरों की अनुपलब्धता का भी संकेत होती है। इस समस्या का समाधान केवल दान या सहायता से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को कौशलयुक्त बनाया जाए, उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया जाए। साथ ही, देश की आर्थिक प्रगति को मात्र आँकड़ों या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मापदंड से नहीं आँका जाना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि उस विकास से समाज में कितना न्याय सुनिश्चित हुआ, पर्यावरण की कितनी रक्षा हुई और मानवीय मूल्यों का कितना विस्तार हुआ है। जब विकास इन सभी दिशाओं में संतुलित रूप से आगे बढ़ेगा, तभी एक ऐसा समाज निर्मित हो सकेगा जो सबके लिए स्थायी, उत्तरदायी और समरस होगा और यही आर्थिक समाजरक्षण की सच्ची उपलब्धि मानी जाएगी।
5. न्यायिक एवं विधिक समाजरक्षण
समाज की बुनियाद में न्याय व्यवस्था एक अत्यंत आवश्यक और केंद्रीय भूमिका निभाती है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि “कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं।” यह सिद्धांत केवल संविधान के पृष्ठों तक सीमित न रहे, बल्कि यह समाज के व्यवहार, सोच और संस्थागत ढाँचे में भी साकार रूप में प्रतिबिंबित होना चाहिए। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष, समान और सुलभ न्याय नहीं मिलेगा, तब तक समाज में विश्वास, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता की भावना विकसित नहीं हो सकती। न्यायिक समाजरक्षण का तात्पर्य है — ऐसा न्यायिक और विधिक ढाँचा तैयार करना जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के उसके अधिकार, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करे। यही सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की मूल शर्त है।
आज समाज में फैली बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, घरेलू हिंसा जैसी अनेक बुराइयों के विरुद्ध बनाए गए कानून ही समाज की रक्षा के कानूनी आधार बनते हैं। किंतु केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता — उनका प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों को उनके अधिकारों की सम्यक जानकारी होना भी उतना ही आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा जैसे मूल अधिकारों की रक्षा केवल सरकार की नहीं, अपितु सम्पूर्ण समाज की साझा जिम्मेदारी है। साथ ही, यदि न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब हो, तो वह भी एक प्रकार का अन्याय बन जाता है। अतः हमारी न्याय प्रणाली को तेज़, सुलभ और संवेदनशील बनाना अत्यंत आवश्यक है। जब प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित हों और समाज में समानता तथा न्याय का भाव सुदृढ़ हो, तभी न्यायिक एवं विधिक समाजरक्षण अपने वास्तविक स्वरूप में साकार हो सकता है।
6. संस्कृतिक समाजरक्षण
संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है, जो उसकी पहचान, सोच और जीवनशैली को दिशा और स्वरूप प्रदान करती है। हमारी भाषाएँ, लोककथाएँ, पारंपरिक नृत्य, संगीत, पर्व-त्योहार और रीति-रिवाज़ मात्र परंपराएँ नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी जीवंत धरोहरें हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमारे सामूहिक अस्तित्व को आधार देती हैं। जब हम इन सांस्कृतिक तत्वों को भुलाने या उपेक्षित करने लगते हैं, तो यह केवल परंपरा का नहीं, बल्कि समाज के आत्मिक और भावनात्मक ताने-बाने का भी ह्रास होता है। अतः संस्कृति का संरक्षण केवल कलाकारों, साहित्यकारों या विद्वानों का दायित्व नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझे, आत्मसात करे और उसे अगली पीढ़ियों तक सम्मानपूर्वक पहुँचाए। यही सांस्कृतिक समाजरक्षण का मूल स्वरूप है, जो समाज को जड़ों से जोड़े रखते हुए भविष्य की ओर उन्मुख करता है।
लोक-संस्कृति समाज की आत्मा और उसकी जड़ों से जुड़ी होती है, जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, नैतिक शिक्षा और जन-जागरूकता का भी सशक्त माध्यम है। आज के दौर में यह आवश्यक हो गया है कि हम इन परंपराओं को आधुनिक जीवन के साथ जोड़ें, ताकि युवा पीढ़ी इन्हें अपनाने में गर्व महसूस करे। आधुनिकता आवश्यक है, लेकिन यदि वह हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ दे, तो समाज अपनी पहचान खो बैठता है। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बना रहे—जहाँ तकनीक और विकास, संस्कृति को नष्ट करने की बजाय उसे संरक्षित करें—तभी हम सच्चे अर्थों में सांस्कृतिक समाजरक्षण कर सकते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में, जब पूरी दुनिया एक-सी होती जा रही है, तब हमारी सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखना और भी आवश्यक हो गया है। भारत की संस्कृति की वास्तविक शक्ति इसकी ‘विविधता में एकता’ की भावना में निहित है और इसी को जीवित रखते हुए हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
7. वैज्ञानिक एवं तकनीकी समाजरक्षण
आज का युग विज्ञान और तकनीक का है, जिसने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे आविष्कारों ने न केवल हमारे सोचने और कार्य करने के तरीकों को बदला है, बल्कि आपसी संपर्क और संवाद के स्वरूप को भी पूरी तरह रूपांतरित कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही वैश्विक समुदाय से जुड़ सकता है और अपनी बात तुरंत व्यापक स्तर पर साझा कर सकता है। परंतु इस तीव्र तकनीकी विकास के साथ कई जटिल चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे—झूठी खबरों का प्रसार, साइबर अपराधों का बढ़ना, व्यक्तिगत सूचनाओं का दुरुपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी। अतः आज यह अत्यंत आवश्यक है कि हम तकनीक का प्रयोग जिम्मेदारीपूर्वक करें, लोगों को इसके विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूक बनाएं तथा डिजिटल नैतिकता और साइबर सुरक्षा की समझ को समाज में स्थापित करें। विज्ञान और तकनीक का उपयोग समाज के कल्याण में हो, न कि उसके विनाश में, यही वैज्ञानिक और तकनीकी समाजरक्षण का मूल उद्देश्य है।
आज विज्ञान और तकनीक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यदि तकनीक का सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो यह समाज को अधिक सशक्त, सुरक्षित और उन्नत बना सकती है। उदाहरणस्वरूप, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और ई-गवर्नेंस जैसी सुविधाएँ आम जनजीवन को सरल और सुलभ बना रही हैं। किंतु इन सभी का उपयोग करते समय नैतिकता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। आज की आवश्यकता है कि समाज को तकनीकी रूप से जागरूक किया जाए, उसे सही जानकारी दी जाए और तकनीकी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सिखाया जाए। विज्ञान और तकनीक यदि सदुपयोग की दिशा में कार्य करें, तो ये समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं; परंतु यदि इनका दुरुपयोग हो, तो यही भ्रम, असमानता और असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। अतः वैज्ञानिक और तकनीकी समाजरक्षण आज के युग की अत्यंत आवश्यक और सामूहिक जिम्मेदारी बन चुका है।
8. पर्यावरणीय समाजरक्षण
आज जब पर्यावरण संकट सम्पूर्ण विश्व के लिए गहन चिंता का विषय बन चुका है, तब प्रकृति की रक्षा केवल किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं रह गई है, बल्कि यह हम सभी की साझी और अनिवार्य ज़िम्मेदारी बन चुकी है। वृक्ष, नदियाँ, पर्वत, पशु-पक्षी – ये केवल पर्यावरण के घटक नहीं, बल्कि हमारे जीवन की मूलभूत जड़ें हैं। यदि जैव विविधता का संतुलन बिगड़ता है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य, जीवनशैली और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। अतः अब पर्यावरणीय समाजरक्षण कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकता बन गया है। हमें प्रकृति को उपभोग की वस्तु मानने की बजाय उसके साथ सह-अस्तित्व का मार्ग अपनाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह गहराई से समझना होगा कि हम प्रकृति से पृथक नहीं, बल्कि उसी का अभिन्न अंग हैं।
जल, वायु और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधन केवल उपभोग की वस्तुएँ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत हैं। यदि हम आज इनका अंधाधुंध दोहन करते हैं, तो हम भविष्य के लिए गंभीर संकट खड़ा कर रहे हैं। इसी चिंतन से “सतत विकास” की अवधारणा जन्मी है, जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की संभावनाओं की भी रक्षा की जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाए। जब बच्चे प्रकृति को समझेंगे, उससे प्रेम करेंगे और उसकी रक्षा की चिंता करेंगे, तभी एक जागरूक और जिम्मेदार समाज का निर्माण संभव होगा। साथ ही, ऐसी नीतियाँ भी बनाई जानी चाहिए जो पर्यावरण-संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और जिनका पालन कठोरता से सुनिश्चित किया जाए। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना और उसे सुरक्षित रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी स्वस्थ और सुखद जीवन जी सकें—यही पर्यावरणीय समाजरक्षण का मूल संदेश है।
9. नैतिक और चारित्रिक समाजरक्षण
किसी भी समाज की असली ताकत उसकी आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास या वैज्ञानिक उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के नैतिक मूल्यों और चरित्र में निहित होती है। सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा और संयम जैसे गुण केवल किसी व्यक्ति के अच्छे स्वभाव का परिचायक नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज की आत्मा होते हैं। यदि समाज में ये मूल्य जीवित हैं, तो वह समाज दीर्घकाल तक टिकाऊ बनता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। महात्मा गांधी ने कहा था, “यदि हम अपने नैतिक मूल्यों को खो देंगे, तो स्वतंत्रता भी खो बैठेंगे।” यह चेतावनी केवल राजनीति के लिए नहीं थी, बल्कि समूचे समाज के लिए थी। जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में सच्चाई, संवेदना और जिम्मेदारी को बनाए रखता है, तब तक समाज की दिशा भी सही बनी रहती है। समाज की वास्तविक सेहत तभी सुरक्षित रह सकती है, जब हर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, आत्मशोधन में प्रवृत्त हो और जिम्मेदारीपूर्वक जीवन यापन करे।
एक व्यक्ति का उत्तम चरित्र ही समाज में श्रेष्ठ आदर्शों की नींव रखता है। समाज एक विशाल वृक्ष के समान है और व्यक्ति उस वृक्ष का बीज यदि स्वस्थ और सुसंस्कारित हो, तो वृक्ष अपने आप फलता-फूलता है। अतः परिवार, संबंधों और समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यदि घर में विश्वास, सहयोग और संवाद का स्वस्थ वातावरण हो, तो बच्चे भी सहज ही सद्गुणों और अच्छे संस्कारों के साथ विकसित होते हैं। भौतिक प्रगति आवश्यक अवश्य है, किंतु यदि वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण और नैतिक चेतना से विमुख हो, तो समाज को केवल बाहर से समृद्ध दिखा सकती है, भीतर से खोखला कर सकती है। एक संतुलित समाज वही कहलाता है, जहाँ विज्ञान के साथ विवेक, तकनीक के साथ नैतिकता और सफलता के साथ आत्मसंयम का समन्वय हो। ऐसा संतुलन ही समाज को न केवल संगठित, बल्कि सुरक्षित, सशक्त और संस्कारित बनाता है — यही नैतिक और चारित्रिक समाजरक्षण का वास्तविक रूप है।
10. समाजरक्षण में व्यक्तित्व और नेतृत्व की भूमिका
समाजरक्षण की दिशा में हमारे देश के अनेक महान समाज सुधारकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उसे समाप्त करवाने में अहम भूमिका निभाई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा-विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने और स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास किए। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों और वंचितों को न्याय, समानता और आत्मगौरव दिलाने हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इन सभी महापुरुषों ने केवल विचार नहीं दिए, बल्कि उन्हें कर्म में ढालकर समाज में गहरे और स्थायी परिवर्तन लाए। उनके उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि जब कोई व्यक्ति संवेदनशीलता, साहस और संकल्प के साथ कार्य करता है, तो वह न केवल अन्याय के विरुद्ध एक चेतना बनता है, बल्कि समूचे समाज की दिशा को बदल सकता है।
आज के समय में समाज निर्माण की ज़िम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक की है — चाहे वह शिक्षक हो या पत्रकार, वैज्ञानिक हो या किसान, डॉक्टर हो या उद्यमी। विशेष रूप से युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही समाज के भविष्य की नींव हैं। जब युवा अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं और राष्ट्रसेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाते हैं, तब ही समाज में समानता, भाईचारा और न्याय की भावना स्थायी रूप से स्थापित हो सकती है। समाजरक्षण का अर्थ केवल बड़े-बड़े आंदोलनों से नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपे नेतृत्व और सेवा-भाव को पहचानकर उसे समाज की भलाई में लगाना ही सच्चा समाजरक्षण है।
11. समाजरक्षण की वर्तमान चुनौतियाँ
आज के समय में समाज को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जाति-पाति का भेदभाव, लिंग के आधार पर भेद, धर्म के नाम पर संघर्ष, और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई जैसी समस्याएँ आज भी समाज की एकता को कमजोर कर रही हैं। तकनीक और इंटरनेट ने जहाँ जीवन को सहज बनाया है, वहीं इससे सामाजिक असमानताएँ और अधिक उजागर हो गई हैं। गरीब और वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित इलाज और न्याय सुलभ नहीं हो पाता, जिससे वे मुख्यधारा से और भी अधिक कट जाते हैं। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर फैलती झूठी खबरें और नफरत फैलाने वाले संदेश समाज में तनाव और वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं।
आज के दौर में लोगों में नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना धीरे-धीरे कम होती जा रही है। नेता भी प्रायः अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जिससे समाज की भलाई पीछे छूट जाती है। युवा वर्ग भले ही बड़ी नौकरियों और सफलता की दौड़ में आगे बढ़ रहा हो, लेकिन समाज सेवा और नागरिक उत्तरदायित्वों से उसका जुड़ाव कम होता जा रहा है। परिवारों का विघटन हो रहा है, बुजुर्गों की उपेक्षा बढ़ रही है और मानसिक तनाव जनसामान्य में गहराता जा रहा है। इन सभी कारणों से समाज की समग्र सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम फिर से इंसानियत, सह-अस्तित्व की भावना और संविधान में प्रतिपादित मूल्यों की ओर लौटें, ताकि समाज को सुदृढ़, सुरक्षित और समरस बनाकर समाजरक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा सकें।
12. समाजरक्षण के उपाय
समाज को सुरक्षित, स्वस्थ और समरस बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा को सशक्त आधार बनाना अत्यावश्यक है। यह शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न होकर, उसमें संस्कार, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश होना चाहिए। जब बच्चे बचपन से ही सत्य, सहनशीलता, समानता और सेवा जैसे मानवीय मूल्यों को आत्मसात करते हैं, तब वे भविष्य में सजग, संवेदनशील और अच्छे नागरिक बनते हैं। इसके साथ ही, समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और अधिकार मिलें — जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, सम्मानजनक रोजगार और न्याय — यह सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। स्त्री-पुरुष समानता को स्वीकारना, जाति-धर्म के भेदभाव से ऊपर उठना, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना — ये सभी उपाय समाज को संतुलित, टिकाऊ और समावेशी बनाने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।
आज के समय में तकनीक और मीडिया समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों का सही उपयोग करके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सत्य जानकारी फैला सकते हैं और भ्रामक बातों का विरोध भी कर सकते हैं। मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज में सकारात्मक सोच, आपसी समझ और समरसता को बढ़ावा दे। इसके साथ ही, गाँवों में पंचायतें, शहरों में नागरिक समितियाँ और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ बनाने की प्रक्रिया में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना विकसित करता है, तभी हम एक बेहतर, सशक्त और सभी के लिए सुरक्षित समाज की रचना कर सकते हैं।
निष्कर्ष
समाजरक्षण कोई एक दिन में पूर्ण होने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो समय के साथ प्रत्येक पीढ़ी को प्रभावित करती है। इसका उद्देश्य केवल जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करना है। जब समाज में सभी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और विचारधारा से जुड़े लोगों को समान महत्व और आदर मिलता है, तभी हम सच्चे अर्थों में समाज को सुरक्षित, समरस और संतुलित बना सकते हैं। समाजरक्षण का उद्देश्य मनुष्य को केवल कानून या नियमों से नहीं, बल्कि आत्मीयता, करुणा और परस्पर सहयोग की भावना से जोड़ना होता है।
समाजरक्षण का मूल भाव “वसुधैव कुटुम्बकम्” में निहित है, जिसका अर्थ है — समस्त संसार एक परिवार है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब समाज के लिए कुछ करना केवल एक दायित्व नहीं रहता, बल्कि यह जीवन का सहज, स्वाभाविक और आत्मीय कर्म बन जाता है। ऐसा समाज, जहाँ न्याय, करुणा और संतुलन विद्यमान हों, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करता है। समाज की मजबूती केवल शासन या नीतियों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होती है। जब सभी मिलकर सहयोग, सहभाव और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं, तभी एक न्यायपूर्ण, सशक्त और समरस समाज की आधारशिला रखी जाती है और यही समाजरक्षण का वास्तविक स्वरूप है।
योगेश गहतोड़ी